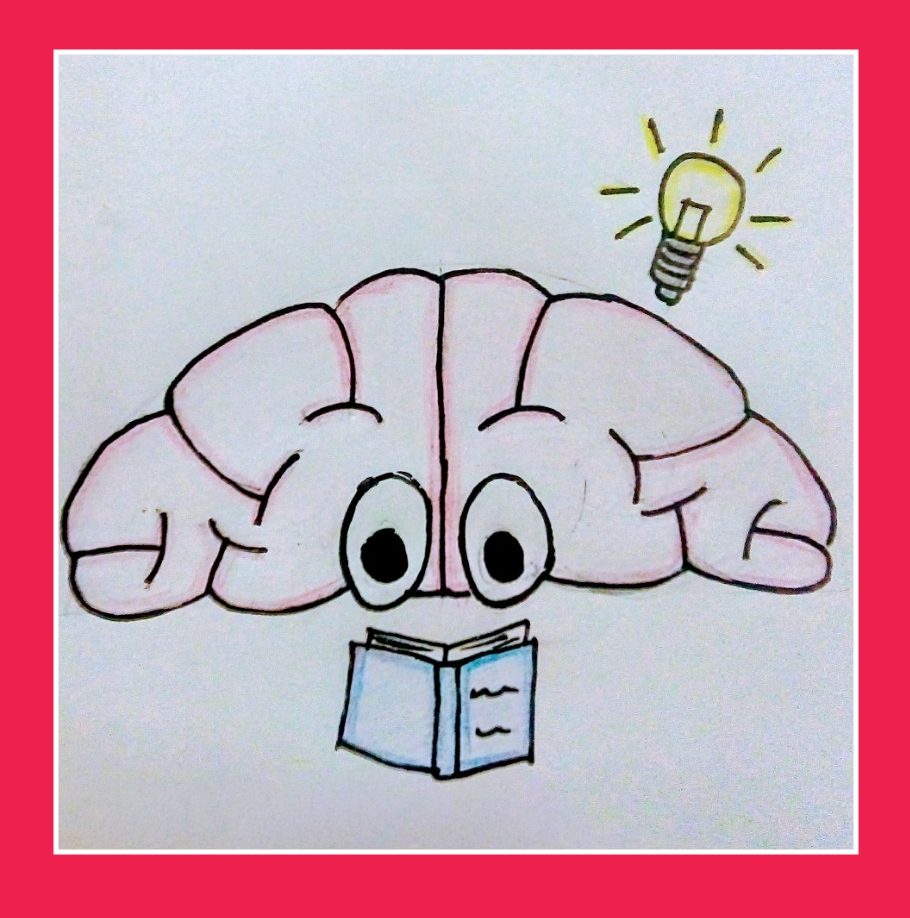बालिग़ हुए तो घर से हम निकले,
क्या करने उसका कुछ ज़्यादा हिसाब ना था।
बन जाएँगे शायद कुछ कहीं पहुँच कर,
किसी मंज़िल पर जा कर कुछ अपना होना था।
घर से निकले तो कई झोले थे,
कुछ हमने, कुछ घर वालों ने बांधे थे।
खील बताशे भरे थे कुछ में,
कुछ में हमने हर मौसम के कपड़े डाले थे,
कुछ में घर का प्यार था, कुछ में घर के ठाठ थे।
कुछ में था रौब, कुछ में बिन ज्ञान के दिमाग़ थे।
कुछ दूर चले हम तो हमें भूख लगी,
बताशे तो कब के ख़त्म थे,
आदत ढेर पकवान की कब की छूटी,
जाने फिर की पेट ईमान की सूखी रोटी से भी भरते।
जाड़े आये, आयी गर्मी, पर पैदल हर मौसम में चलते रहते,
थके इतना कि बिस्तर बनाने का भी होश नहीं,
जहां लेटे, वहीं बस सोते।
दौड़े खूब पहले, आगे निकलने की होड़ थी,
पर समय के साथ जाने, ये तो कोई दौड़ थी ही नहीं।
दिन काम से भरे पर दिमाग़ ख़ाली, ऐसी परवरिश तो थी नहीं,
तो सुनते गुनगुनाते इन रास्तों के राग, ज़िंदगी अच्छा बुरा सिखाने लगी।
जो रौब हमने कहीं से ले लिया था,
खुले आसमाँ ने सिखाया, वो तो हमने उधार लिया था,
इन्ही चाँद तारों ने सैकड़ों को बनते मिटते देखा,
हमने थोड़ा ज्ञान कमा कर कुछ अलग थोड़े किया था।
उन झोलों का भार हल्का जैसे जैसे हुआ,
चाल तेज़, और मन मानो कुछ शांत हुआ।
अब झोलों में हमने गीत भरे,
कुछ सबक़ के, कुछ सब्र के भरे।
और अब जब हम घर लौटे,
और माँ पूछी, बताओ क्या बने?
माँ, हम इंसान बने।
Grain for Brain